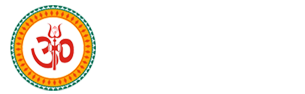शुद्ध श्रीमद्भगद्गीता में भगवान अर्जुन को अध्याय 2 के श्लोक 16 से 30 तक सत् (Eternal Essence of the Universe) का ज्ञान देते हैं। इसे ही श्रीमद्भगवद्गीता में ‘ज्ञानयोग’ कहते हैं। अर्जुन के समक्ष सबसे बड़ा संकट यह है कि वो आखिर युद्ध करे तो कैसे करे? वो अपने ही स्वजनों के रक्त से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। वो अपने स्वजनों के संभावित वध से चिंतित है । इस चिंता के अलावा अर्जुन करुणा से भरा हुआ है। अर्जुन को लगता है कि अपने स्वजनों के वध से जो पाप लगेगा, वो उसे और उसके कुल को नरकगामी बना देगा ।
इसी मोह से ग्रस्त होकर वो युद्धकर्म का त्याग कर देता है और युद्ध से पलायन कर जाता है। इसीलिए भगवान सबसे पहले उसे सत् (Eternal Essence of the Universe) का सिद्धांत देते हैं। भगवान उससे कहते हैं कि “कोई किसी को नहीं मारता। केवल शरीर की मृत्यु होती है। इस शरीर के अंदर स्थित अविनाशी या नित्य शरीरी या सत्(Eternal Essence of the Universe) को कोई नहीं मारता और यह अमर है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम इनकी हत्या कर दोगे और इसलिए युद्ध से पलायन कर रहे हो तो यह तुम्हारा भ्रम है।”
श्रीमद्भगवद्गीता का सांख्ययोग क्या है?
शुद्ध श्रीमद्भगवद्गीता में पहले भगवान सत् (Eternal Essence of the Universe) को अविनाशी बता कर अर्जुन के संशय को दूर करते हैं। इसके बाद वो अर्जुन को अध्याय 2 के श्लोक 31 से 38 तक युद्ध के लिए वापस खड़ा होने के लिए कहते हैं। भगवान अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हैं और कहते हैं कि” इस पलायन को छोड़कर क्षत्रिय धर्म युक्त कर्म को करने के लिए तत्पर हो जाओ।”
एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु ।
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥2.39॥
ēṣā tē.bhihitā sāṅkhyē buddhiryōgē tvimāṅ śrṛṇu.
buddhyāyuktō yayā pārtha karmabandhaṅ prahāsyasi৷৷2.39৷৷
अर्थ: “हे पार्थ ! यह बुद्धि तूझे सांख्य के विषय में कह दी गई, अब कर्मयोग के विषय में उसे ( यानि कर्मविषयक बुद्धि को ) सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन का भलीभांति त्याग कर देगा।”
व्याख्याः- भगवान यहां अर्जुन से कह रहे हैं कि” मैंने तेरे उस संशय को दूर करने का प्रयास किया, जिसमें तू यह समझ रहा था कि तू अपने स्वजनो की हत्या का अपराधी होगा । अपने स्वजनों की हत्या का तूझे पाप लगेगा , जबकि वास्तव में सत्य यही है कि कोई किसी को नहीं मार सकता और न कोई किसी के द्वारा मारा जा सकता है।” अर्जुन को लगता है कि युद्ध कर्म के फलस्वरुप वो जो भी हत्याएं करेगा उसका पाप उसके साथ बंध जाएगा। वो इस पापकर्म के बंधन से बंध जाएगा।
भगवान कहते हैं कि “जिन शरीर रुपी अपने स्वजनों की संभावित हत्या से तूझे मोह रुपी भ्रम हो रहा है , उनके अंदर वही अविनाशी सत्(Eternal Essence of the Universe) है जो न तो किसी के द्वारा मारा जा सकता है और न ही कोई उसे मार सकता है । यह अविनाशी सत्(Eternal Essence of the Universe) नित्य और अमर है।”
भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि “अब मैं तुम्हें जिस ज्ञान को बताने जा रहा हूं इससे तुम अपने कर्म बंधन का त्याग कर दोगे।” वास्तव में अर्जुन का संशय यही है। वह युद्ध कर्म करना ही नहीं चाहता ।अपने स्वजनों की हत्या का कर्म उसे पापकर्म लगता है । भगवान जानते हैं कि यही मोह का बंधन उसे कर्म करने से रोक रहा है । इसलिए इस मोह को दूर कर ही उसे कर्म के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
भगवान अध्याय 2 के श्लोक 11 से 30 तक में दिए गये ज्ञान को ‘सांख्ययोग’ की संज्ञा देते हैं। ‘एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये..’। बुद्धि का नाम संख्या है, इसलिए बुद्धि से धारण होने वाले आत्मतत्व का नाम सांख्य है। जैसे ही हम बुद्धि के स्तर पर चेतन होते हैं, हम खुद को संख्याओंसे घिरा पाते हैं। सुख- दुख, अच्छा- बुरा, मधुर -कटु, पाप-पुण्य ये द्वंद्वात्मकता ( ड्यूलिज्म या Duality) हमारी चेतना को घेर लेती है। हम इन दो संख्यात्मक भावो में अपनी पूरी जिंदगी तय करते हैं।
भगवान ने एक अविनाशी सत् (Eternal Essence of the Universe) का ज्ञान देकर अर्जुन की इसी संख्यात्मक बुद्धि को अपने सांख्य दर्शन के द्वारा दूर करने के लिए उपदेश दिया। भगवान ने अर्जुन की चेतना को संख्यात्मक बुद्धि से परे ले जाकर एक अविनाशी सत्(Eternal Essence of the Universe) की तरफ प्रेरित किया। अर्जुन इसी पाप- पुण्य, सुख-दुख, लाभ-हानि और जय-पराजय के द्वंद्वात्मकता से घिरा हुआ था। भगवान उसे इसके पार ले जाते हैं और बताते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड या सृष्टि संख्याओं से परे है।
जब अविनाशी सत्(Eternal Essence of the Universe) माया का आवरण लेता है तब वो खुद को संख्याओं में प्रगट करता है। छांदोग्य उपनिषद् की उद्घोषणा है -‘एकोहं बहुस्याम’ अर्थात् “मैं एक अनेक रूप में हुआ हूँ। ” ऋग्वेद का नासदीय सूक्त कहता है कि ‘उस एक’ ( That one) के अंदर काम की इच्छा हुई और उसने स्वयं को इस सृष्टि के रुप में प्रगट किया। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि” हम सभी उस एक (That One) के प्रगट सत् रुप ही हैं। कोई किसी को नहीं मारता , कोई किसी को मार नहीं सकता ।”
श्रीमद्भगवद्गीता में कर्म योग के त्याग का ज्ञान : :
भगवान अब उस चेतन बुद्धि को कर्मनुष्ठान में लगाने के लिए अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देने जा रहे हैं।
यनेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवातो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥2.40॥
nēhābhikramanāśō.sti pratyavāyō na vidyatē.
svalpamapyasya dharmasya trāyatē mahatō bhayāt৷৷2.40৷৷
अर्थः- “यहां( इस कर्म योग में) आरंभ का नाश नहीं है और प्रत्यवाय( उल्टा फलरुप दोष) भी नहीं है। उसका (कर्म योग रुपी धर्म का) थोड़ा सा भी अंश बड़े भारी भय से रक्षा कर लेता है।”
व्याख्याः- भगवान यहां अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस कर्म योग को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है और इसके बीच में खत्म हो जाने पर भी कोई दोष नहीं लगता ।अर्थात् अगर किया गया कर्म बीच में ही खत्म हो जाए तो भी इसके फल का नाश नहीं होता।
कर्म क्या है और यह अविनाशी कैसे है? :
इस श्लोक को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान किस कर्म की बात कह रहे हैं। भगवान जिस कर्म की बात कह रहे हैं वो सत् अर्थात अविनाशी नित्य शरीरी के प्रति किये गए कर्म की बात कह रहे हैं। सत् अर्थात अविनाशी जब नाशरहित है तो फिर इसके प्रति किया गया कर्म भी नाशरहित ही होगा , वो अविनाशी ही होगा। इसलिए इस कर्म के आरंभ करते ही यह अविनाशी हो जाता है।
सकाम कर्म किसे कहते हैं? :
सामान्यतः हम जिस कर्म को करते हैं वो लौकिक या सकाम कर्म होते हैं। इसमें कर्म के फल या परिणाम के प्राप्ति की आकांक्षा होती है। जैसे हम नौकरी करते हैं तो इस आशा से करते हैं कि माह के अंत में हमें इस कर्म के फलस्वरुप वेतन की प्राप्ति होगी। हम कोई युद्ध करते है तो इस आशा से करते हैं कि अगर हम विजयी हुए तो हमें राज्य सुख की प्राप्ति होगी या फिर वीरगति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा।
परंतु सत् या अविनाशी सत्ता की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म का फल या परिणाम, सत् या अविनाशी सत्ता की प्राप्ति ही है। इस कर्म योगको प्रारंभ करने वाले को पहले उस अविनाशी सत् का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए भगवान ने पहले अर्जुन को अविनाशी सत् का ज्ञान कराया ताकि वो इसके प्राप्ति हेतु ज्ञानयोग युक्त कर्म कर सके ।
ज्ञानयुक्त कर्म को ही कर्म योग कहते हैं :
- ज्ञानयोग युक्त कर्म ही कर्म योग है। उसी कर्म को कर्म योग की श्रेणी में रखा जा सकता है जो अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए किया जाए। अगर इस प्रकार के कर्म योग को करने में हमारी चेतना का उस अविनाशी सत् से संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर ये संबंध निरंतर बना रहता है। कर्म के रुक जाने के बाद भी यह संबंध खत्म नहीं होता। कर्म खत्म भी हो जाए तो सत् से संबंध स्थापित होने की वजह से उसकी अमरता का भाव बना रहता है और मोह और भ्रम रुपी भय वापस चेतना में नहीं आते।
- इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ” इसमें आरंभ का नाश नहीं है।” अर्थात कर्म योग के द्वारा अविनाशी सत् से संपर्क होने के बाद इसका फल (अविनाशी सत् से संबंध) ज्यों का त्यों बना रहता है। बीच में रोक देने से भी इसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता । लेकिन अगर हम कोई सकाम कर्म करते हैं जैसे बीच में ही नौकरी छोड़ देते हैं तो हमें उसके फलरुपी वेतन की प्राप्ति नहीं होती है।
- अजामिल ने एक बार नारायण का नाम लिया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। केवट ने एक बार श्रीराम के चरण पखारे तो उसे मोक्ष मिल गया । चरण पखारने के बाद हो सकता है कि केवट वापस सांसारिक कर्मो में लिप्त हो गया हो, लेकिन ईश्वरीय सत्ता के स्वरुप श्रीराम के चरणों को एक बार धोने के बाद उसके पुण्य का नाश नहीं हुआ । उसके द्वारा अविनाशी सत् के प्रति किये गए छोटे से कार्य का भी फल उसे अविनाशी सत् की प्राप्ति कराने वाला ही हुआ ।
श्रीमद्भगवद्गीता में निश्चयात्मक बुद्धि का सिद्धांत :
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।
बहुशाका ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥2.41॥
vyavasāyātmikā buddhirēkēha kurunandana.
bahuśākhā hyanantāśca buddhayō.vyavasāyinām৷৷2.41৷৷
अर्थः- “हे कुरुनंदन ! इस कर्म में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक होती है, निश्चयहीन व्यक्ति की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं।”
व्याख्याः- भगवान यहां अर्जुन को एक ऐसी बुद्धि या चेतना के बारे में बता रहे हैं जिसे वो ‘व्यवसायात्मिक बुद्धि’ कह रहे हैं। कर्म योग में इसे ही ‘निश्चयात्मिकता बुद्धि’ भी कहते हैं। चेतना जब बुद्धि और मन के स्तर पर उतरती है तो वो संख्याओं में बंट जाती है। बुद्धि सुख-दुख, पाप- पुण्य, लाभ- हानि , मधुर- कटु आदि द्वंद्वात्मक स्थितियों में बंट जाती है।
सकामी मनुष्य की बुद्धि अनेक शाखाओं में बंट कर विभिन्न परिणाणों पर विचार करने लगती है। मनुष्य इसी द्वंद्वात्मक बुद्धि की वजह से अनंत वस्तुओं, विचारों और परिणामों में फंस कर रह जाता है। कर्म योग में इसे ‘अनिश्चयात्मक बुद्धि’ कहते हैं। सकामी मनुष्य अगर ईश्वर की अराधना भी करता है तो उसके परिणाम स्वरुप संतान प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति जैसे अनंत परिणामों की कामना में लग जाता है। परंतु व्यवसायात्मिकता युक्त बुद्धि सिर्फ एक होती है। अविनाशी सत् की प्राप्ति के लक्ष्य का ज्ञान ही मनुष्य की बुद्धि को एक करता है । एक बुद्धि से तात्पर्य है एक सत् की प्राप्ति के लिए केंद्रित बुद्धि । ऐसी बुद्धि ही निश्चयात्मक होती है।

श्रीमद्भगवद्गीता में निश्चयात्मक बुद्धि और व्यवसायात्मिक बुद्धि का सिद्धांत :
निश्चयात्मक बुद्धि के लिए भगवान ने व्यावसायात्मिक बुद्धि की संज्ञा ही है। व्यावसाय अर्थात फल की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म । जब फल या परिणाम अविनाशी सत् हो तो फिर ऐसी बुद्धि तो एक ही परिणाम की प्राप्ति के लिए कर्म करेगी। सबसे बड़ा व्यावसायिक कर्म परम सत्ता रुपी अविनाशी सत् की ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म है। जब सत् एक है, इसका फल भी अविनाशी सत् की प्राप्ति है तो फिर इसके लिए किये जाने वाले कर्म में लगी बुद्धि भी एक होगी , अर्थात निश्चयात्मक ही होगी।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥2.42॥
yāmimāṅ puṣpitāṅ vācaṅ pravadantyavipaśicataḥ.
vēdavādaratāḥ pārtha nānyadastīti vādinaḥ৷৷2.42৷৷
अर्थः- हे पार्थ( स्वर्ग परायण)! केवल फलश्रुत में रत ( यानि वेदों में जो स्वर्गादि फलों को बताने वाले वाक्य हैं, उनमें रत) अज्ञानी अल्पज्ञ, इससे ( स्वर्गादि सुखों से) बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा जिस पुष्पित (सुहावनी) वाणी को कहा करते हैं ।।2.42।।
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविश्लेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥2.43॥
kāmātmānaḥ svargaparā janmakarmaphalapradām.
kriyāviśēṣabahulāṅ bhōgaiśvaryagatiṅ prati৷৷2.43৷৷
अर्थः- “विषयासक्त ,स्वर्ग परायण ( अल्पज्ञ मनुष्य) , पुनर्जन्मरुप कर्मफल देने वाली , भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए
भांति – भांति की बहुत सी क्रियाओं से युक्त जिस ऐसी पुष्पित (सुहावनी) बात को कहा करते हैं” ।।2.43।।
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥2.44॥
bhōgaiśvaryaprasaktānāṅ tayāpahṛtacētasām.
vyavasāyātmikā buddhiḥ samādhau na vidhīyatē৷৷2.44৷৷
अर्थः- “उस (यानि सुहावनी ) वाणी से अपह्रत (हर लिए गए) चित्त वाले, भोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त मनुष्यों में निश्चयात्मिकता बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है”।।2.44।।
व्याख्याः- भगवान अर्जुन से यहां कह रहे हैं कि अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए किये गए कर्म के अलावा जितने भी सकाम कर्म हैं उसे करने से निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। भगवान ने गीता के अध्याय 2 के 42वें , 43वें और 44 श्लोकों में सकाम भावना से युक्त वैसे वेदोक्त धार्मिक कर्मों का वर्णन किया है, जिसे अल्पज्ञ और अज्ञानी लोग अपनी सुहावनी बातों से कहा करते हैं।
भगवान केवल फलश्रुत (यानि किसी कार्य के परिणाम स्वरुप जिसकी प्राप्ति होती है) कार्यों में रत रहने वालों को अज्ञानी और अल्पज्ञ कहते हैं। भगवान के अनुसार ये अज्ञानी लोग वेदों का सहारा लेकर स्वर्ग प्राप्ति और अन्य सुखों के बारे में बताते हैं।
श्रीमद्भगवद्गीता में वेदों का मूल अर्थ छिपा है?
भगवान के अनुसार ऐसे लोग वेदों के सतही ज्ञान से युक्त होकर ऐसी उपासना , पूजा, यज्ञ आदि बताते हैं, जिनसे स्वर्ग आदि सुख मिल सकते हैं। ऐसे अज्ञानी विषयासक्त करने वाली बाते बताते हैं। जैसे – इस यज्ञ को करने से संतान की प्राप्ति होगी, इस यज्ञ को करने से राज्य की प्राप्ति होगी, इस पूजा को करने से धन की प्राप्ति होगी। ये अज्ञानी इसके लिए वेदों की ऋचाओं का हवाला देते हैं।
ये अज्ञानी ऐसी पूजा पद्धतियों के प्रचार करते हैं, जिनके करने से पिछले जन्मों के बंधन कट जाते हैं, एक उच्च योनि में पुनर्जन्म हो सकता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी और अल्पज्ञ ज्ञानी अपनी मीठी- मीठी बातों से सामान्य मनुष्य का चित्त हर लेते हैं, और भोगों और ऐश्वर्य की तरफ मोड़ देते हैं।
श्रीमद्भगवद्गीता वेदों का रहस्य प्रगट करती है
- भगवान कहते हैं कि इन अज्ञानियों की मीठी- मीठी वैदिक तार्किक बातों से सामान्य मनुष्य का चित्त भ्रमित हो जाता है और वो अविनाशी सत् की प्राप्ति की तरफ अपनी निश्चयात्मक बुद्धि को नहीं लगा पाता । ऐसे आसक्त और भ्रमित मनुष्यों में सत् की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाती
- ऐसा लगता है कि भगवान वेदों में बताई गई उपासना पद्धतियों का उपहास कर रहे है और इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है । भगवान का कहना है कि ऐसे अल्पज्ञ और अज्ञानी लोग वेदों के मंत्रों का विद्वान होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन वो वेदों के तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं ।
- भगवान कह रहे हैं कि वेदों में भी अविनाशी सत् की प्राप्ति को लेकर किये गए कर्मों का ही वर्णन है। बस ये अल्पज्ञ और अज्ञानी लोग इसके तत्व ज्ञान को नहीं समझ कर बस इसके शाब्दिक अर्थों से ही इसे जानते हैं और अन्य दूसरे मनुष्यों का चित्त हर कर उन्हें भी भ्रमित कर देते हैं।
भगवान श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 15 के श्लोक 15 में कहते हैं कि-
‘वदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः’ अर्थात् “संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं।” लेकिन अल्पज्ञ और अज्ञानी सिर्फ वेदों के शब्दार्थों को पकड़ कर उसके तत्वज्ञान को खुद भी नहीं समझ पाते और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं।
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥2.45॥
traiguṇyaviṣayā vēdā nistraiguṇyō bhavārjuna.
nirdvandvō nityasattvasthō niryōgakṣēma ātmavān৷৷2.45৷৷
अर्थः- “हे अर्जुन ! वेद तीनों गुणों ( सत्व, रजस और तम) वाले मनुष्यों को विषय करने वाले हैं, तू इन तीनों गुणों की अधिकता से रहित, सदा सत्वगुण में स्थित, समस्त द्वंद्वों से अतीत और योग ( सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति) तथा क्षेम ( उनकी रक्षा) को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो जाओ।”
व्याख्याः- भगवान यहां अर्जुन को कह रहे हैं कि वेदों के मूल तत्व को वही जान सकता है जो तीनों गुणों ( सत्व , रजस और तमस) की अधिकता से रहित हो, सदा सत्वगुण में स्थित हो, और समस्त द्वंद्वों से परे ( अर्थात सुख- दुख, लाभ- हानि, जय- पराजय, मधुर- कटु) हो । गीता में सत् को अविनाशी और नित्य शरीरी बताया गया है। सत् जब त्रिगुणात्मक (सत्व , रजस् और तम ) रुपी माया के आवरण में प्रवेश करता है तो संसार में व्यष्टि और सृष्टि का निर्माण होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सत्व, रज और तम रुपी तीन गुणों के आवरण से बना है, जिसे माया भी कहते हैं।
इसी माया के आवरण में जब अविनाशी सत् का प्रवेश होता है तो समस्त सृष्टि का निर्माण होता है । समस्त पदार्थ और प्राणी इसी तीन गुणों से घिरें हैं जिसे भगवान ने अनित्य और नाशवान की संज्ञा दी है। इसी नाशवान जीवन जगत के प्रपंच को माया भी कहते हैं। हमारा शरीर इसी अनित्य और नाशवान त्रिगुणात्मक माया के आवरण से बना है जिसके अंदर अविनाशी सत् का वास है ।
सत्व गुण से ही अविनाशी सत् की प्राप्ति संभव है :
भगवान अर्जुन को पहले ही अविनाशी सत् का ज्ञान दे चुके हैं। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि “इस तीनों गुणों से युक्त नाशवान शरीरों ( भीष्म, द्रोण आदि) और पदार्थों के प्रति अपने मोह का त्याग करो और इसकी रक्षा करने के भाव से मुक्त हो जाओ।” भगवान कहते हैं कि” इससे मुक्त होकर तुम आत्मपरायण अर्थात खुद को अविनाशी सत् के रुप में जान कर उसके प्रति स्थित हो जाओ।”
भगवान अर्जुन को इसके लिए तीनों गुणों में से एक सत्व गुण को ही सदा धारण करने के लिए कहते हैं क्योंकि सत्व गुण ही अविनाशी सत् की प्राप्ति में सहायक है। वेद के मूल तत्व को भी सत्व गुण से ही जाना जा सकता है। बाकि के दो गुण रजस और तमस व्यक्ति को सांसारिक कर्म की तरफ प्रेरित करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो तीनों गुणों से घिरा रहता है, उसे वेद का मूल ज्ञान कभी समझ नहीं आता । तीनों गुणों से युक्त मनुष्य वेदों से भी उन्हीं बातों को ग्रहण कर लेता है जो सकाम फल रुपी विषयों से संबंधित हैं।
यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके ।
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥2.46॥
yāvānartha udapānē sarvataḥ saṅplutōdakē.
tāvānsarvēṣu vēdēṣu brāhmaṇasya vijānataḥ৷৷2.46৷৷
अर्थः- “सब ओर से पूर्ण जलाशय में (प्यासे को जितनी जरुरत है उतना ही पानी लेता है) वैसे ही वेदविद्( या तत्वज्ञ) ब्राह्मण को सभी वेदों में उतना ही ग्रहणीय है जितना अंश आवश्यक हो।”
व्याख्याः- भगवान अर्जुन को कहते हैं कि “जिस प्रकार पूर्ण जलाशय में बहुत सा पानी भरा रहता है, लेकिन प्यासे को जितनी जरुरत होती है वो उससे उतना ही पानी लेता है। ठीक इसी प्रकार वेदों में अनंत बातें कही गई हैं, लेकिन वेदों का वास्तविक जानकार या जिसे मूल तत्व का ज्ञान है , वह वेदों से उसी मूल तत्व को ही ग्रहण करता है, बाकि के अंश को वो छोड़ देता है ।
वेदों में आम जीवन के बारे में भी बहुत सी बातें कही गई है। वेदों में अश्व, गो, धन आदि की प्राप्ति को लेकर भी प्रार्थनाएं हैं। वेदों में युद्ध और लोभ की भी कथाएं हैं। लेकिन साथ ही वेदों में अविनाशी सत् के बारे में भी कहा गया है। जो ब्रह्म अर्थात अविनाशी सत् को जानने वाला है ( ब्राह्मण) वह वेदों से सिर्फ मूल तत्व अर्थात अविनाशी सत् से संबंधित ही ज्ञान लेता है और सकाम कर्मों के बारे में दिए गए ज्ञान को छोड़ देता है।
अविनाशी सत् की प्राप्ति हेतु किया गया प्रयास ही कर्म है :
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥2.47॥
karmaṇyēvādhikārastē mā phalēṣu kadācana.
mā karmaphalahēturbhūrmā tē saṅgō.stvakarmaṇi৷৷2.47৷৷
अर्थः- “तेरा कर्म में ही अधिकार है, फलों पर कभी नहीं। कर्मफल का हेतु मत हो तथा अकर्म ( कर्म नहीं करने) में तेरी आसक्ति न हो।”
व्याख्याः- यह गीता के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, उपयोग में लाए गए और सबसे ज्यादा ना समझे गए श्लोकों में एक है । ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि इस श्लोक में किसी भी कार्य को करने में परिणाम या फल की प्राप्ति की आकांक्षा का त्याग करने के लिए कहा गया है। इसे ही निष्काम कर्म की संज्ञा दे दी गई है, जिसके अनुसार सामान्य जिंदगी में भी जो हम कर्म करते हैं, उसमें फल की इच्छा न करें। सामान्य कर्मों जैसे नौकरी, युद्ध, खेल आदि लौकिक कर्मों में फल की आकांक्षा के त्याग की बात कही जाती है।
कई फिल्मों में भी इस श्लोक के अर्थों का अनर्थ किया गया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी इस श्लोक में बताए गए कर्म को लौकिक कर्मों से ही जोड़ा जाता है। परंतु वास्तव में यह एक बहुत बड़ा भ्रम है और इस श्लोक के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है और इसके अर्थ का अनर्थ किया गया है।
लौकिक कर्म और कर्म योग में अंतर :
भगवान यहां अर्जुन से जिस कर्म को करने की बात कह रहे हैं, वो लौकिक कर्म नहीं है, बल्कि सत् की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला कर्म है। भगवान ने अध्याय 2 के श्लोक 16 से 30 तक जिस सांख्ययोग के ज्ञान के द्वारा अविनाशी नित्य शरीरी सत् के बारे में अर्जुन को बतलाया है, भगवान उसी अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले कर्म की बात कह रहे हैं।
भगवान ने इस श्लोक से पहले के श्लोक 2.46 में अर्जुन को आत्मपरायण अर्थात अपनी चेतना या बुद्धि के प्रति परायण होने के लिए कहा है। भगवान ने अर्जुन को अध्याय 2 के श्लोक 39 में बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु कह कर निश्चयात्मक बुद्धि को प्राप्त करने का निर्देश दिया है । भगवान ने अर्जुन को व्यासायात्मिकता युक्त बुद्धि (अर्थात वह बुद्धि जो सिर्फ सत् की प्राप्ति में लगे) से युक्त होने और अन्य सकामी कार्यों (जिसमें लौकिक परिणामों की प्राप्ति की आकांक्षा हो) में लगी असंख्य शाखाओं वाली बुद्धि का त्याग करने के लिए कहा है ।
भगवान ने यहां अर्जुन को जिस कर्म के बारे में ज्ञान दिया है वो निश्चयात्मिक बुद्धि युक्त वैसा कर्म है जो अविनाशी सत् की प्राप्ति करने हेतु किया जाता है न कि सकामी कर्म जिसमें फल प्राप्ति की आकांक्षा होती है। इसलिए भगवान जिस कर्म योग की बात कह रहे हैं वो लौकिक जीवन में किए जाने वाले दैनिक कर्मों से एकदम अलग है।
श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार कैसे कर्म करें ? :
चूंकि अविनाशी सत् की प्राप्ति का परिणाम भी अविनाशी सत् ही है, इसलिए इससे लौकिक फलों या परिणामों की प्राप्ति नहीं हो सकती । अविनाशी सत् के लिए किये गए कर्म का परिणाम पूर्ण अविनाशी सत् का ज्ञान ही है । इस लिए भगवान कहते हैं कि तूझे सिर्फ इस अविनाशी सत् की प्राप्ति हेतु अपने अंदर स्थित सत् की ओर ज्ञानयुक्त होकर मार्गशील होना है अर्थात् आत्मपरायण होना है।भगवान अर्जुन को इस आत्मपरायण युक्त होकर किए गए सत् की प्राप्ति हेतु किया गया कर्म को करने के लिए ही कह रहे हैं और इसके कर्मफल का हेतु न होने के लिए निर्देशित भी करते हैं।
श्रीमद्भगवद्गीता में कर्म और अकर्म का सिद्धांत :
भगवान यह भी कहते हैं कि ‘अकर्म’ में तेरी आसक्ति न हो। अकर्म क्या है ? भगवान अकर्म के प्रति अर्जुन को आसक्त न होने के लिए क्यों कह रहे हैं?श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान जिस ‘अकर्म’ की बात कह रहे हैं वो कर्महीनता नहीं है। भगवान ने अध्याय 2 के श्लोक 16-30 में जिस सत् की प्राप्ति का ज्ञान दिया है, उसे उन्होंने सांख्ययोग या ज्ञानयोग का नाम दिया है।
इस ज्ञानयोग को प्राप्त करने के लिए सिर्फ अपनी बुद्धि और चेतना को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जैसे ही हमारी चेतना को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सारी सृष्टि, पदार्थो और प्राणियों का मूल वही अविनाशी सत् है फिर वो प्रज्ञावान हो जाता है और मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है । लेकिन सिर्फ इसे जान लेने से ही अविनाशी सत् की प्राप्ति नहीं हो जाती बल्कि इसके लिए भी कर्म करना पड़ता है।
ज्ञानयोग के प्रति निष्ठा ही ‘अकर्म’ है :
अपनी चेतना को इस स्तर पर जागृत करना इतना सरल नहीं होता । हालांकि इस चेतना को जागृत करने के लिए किसी प्रकार के कर्म की जरुरत नहीं होती । भगवान अविनाशी सत् के ज्ञान का अहसास हो जाने को ही ‘अकर्म’ का नाम देते हैं। लेकिन सिर्फ अहसास हो जाने से ही अविनाशी सत् की प्राप्ति नहीं हो सकती ।
हम यह सुन कर यह अहसास कर सकते हैं कि अमेरिका एक विशाल देश है परंतु अमेरिका की विशालता को ठीक प्रकार से जानने और समझने के लिए हमें अमेरिका जाना आवश्यक होता है। हमें अमेरिका जाकर वहां भ्रमण का कर्म करना होता है। सिर्फ अमेरिका के बारे मे जान लेना अकर्म है जबकि अमेरिका जाकर वहां भ्रमण कर उसे जानना कर्म है।
अकर्म से कर्म करना श्रेष्ठ है :
भगवान ने अर्जुन को अविनाशी सत् के संबंध में ज्ञान तो दिया लेकिन वो जानते हैं कि अर्जुन इसे बिना कर्म किए प्राप्त नहीं कर सकता, सांख्ययोग के द्वारा अविनाशी सत् का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी कर्म के की आवश्यकता पड़ती है।भगवान अर्जुन को इसीलिए यह कह रहे हैं कि वो ‘अकर्म’ अर्थात ज्ञानयोग के प्रति आसक्ति या निष्ठा न रखे बल्कि अपने क्षत्रिय गुणों के अनुसार कर्म करे । वह कर्म उसे अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए करना है, जिसका फल भी अविनाशी सत् की प्राप्ति ही है। सिर्फ जान लेने रुपी ‘अकर्म’ से उसे कुछ भी नहीं हासिल होगा ।
भगवान गीता के अध्याय 3 के श्लोक 4 और 5 में अकर्म या निष्कर्मता की परिभाषा देते हुए कहते हैं –
न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥
na karmaṇāmanārambhānnaiṣkarmyaṅ puruṣō.śnutē.
na ca saṅnyasanādēva siddhiṅ samadhigacchati৷৷3.4৷৷
अर्थः- “मनुष्य न तो कर्मों के अनारंभ से निष्कर्मता ( ज्ञानयोग के प्रति निष्ठा) को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग से ही सिद्धि को प्राप्त होता है।” (गीता 3.4)
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥
na hi kaśicatkṣaṇamapi jātu tiṣṭhatyakarmakṛt.
kāryatē hyavaśaḥ karma sarvaḥ prakṛtijairguṇaiḥ৷৷3.5৷৷
अर्थः- “क्योंकि, कोई पुरुष किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि परवश हुए सभी से प्रकृतिजनित गुणों के द्वारा कर्म करवाया ही जाता है।”(गीता 3.5)
व्याख्याः- भगवान यहां स्पष्ट रुप से कह रहे हैं कि कर्मों को किए बिना ज्ञानयोग की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है और न ही कर्मों को त्याग कर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जैसे ही हम संसार में जन्म लेते है हमें भूख, प्यास जैसी प्राकृतिक समस्याएं झेलनी ही पड़ती है और हमें इनके लिए कर्म करना ही पड़ता है। कर्म के बिना शरीर की यात्रा असंभव है : भगवान गीता के अध्याय 3 के श्लोक 8 में इसे और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि –
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥
niyataṅ kuru karma tvaṅ karma jyāyō hyakarmaṇaḥ.
śarīrayātrāpi ca tē na prasiddhyēdakarmaṇaḥ৷৷3.8৷৷
अर्थः- “नियत कर्म को करो क्योंकि अकर्म( ज्ञान निष्ठा) की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है और अकर्म से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी।”
व्याख्याः- भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि “जिस ज्ञानयोग को मैंने तुम्हें अध्याय 2 के श्लोक 16-30 में समझाया है, उसके प्रति सिर्फ निष्ठा रखना ‘अकर्म’ है और इससे बेहतर है कि तुम उसी अविनाशी सत् का जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करो जो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि सिर्फ जान कर और निष्ठा रख कर अगर तुम बैठ गए तो इससे तुम्हारे शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी ।
हरेक प्राणी के जन्म लेने का एक उद्देश्य है :
सनातन धर्म में प्रत्येक प्राणी के जन्म का एक उद्देश्य होता है । प्रत्येक प्राणी के जीवन का लक्ष्य उसी अविनाशी सत् की प्राप्ति है जिससे उसका आविर्भाव हुआ है। अविनाशी सत् में वापस विलीन होने की स्थिति को ही मोक्ष कहा गया है। प्रत्येक प्राणी उसी अविनाशी सत् का मूल है और त्रिगुणात्मक (सत्, रज और तम) माया के आवरण में आकर असत् रुपी अनित्य शरीर को धारण करता है।
अलग- अलग जन्मों में और अलग- अलग योनियों ( 84 लाख ) में भटकते हुए प्राणियों के अंदर स्थित अविनाशी सत् का अंश त्रिगुणात्मक माया के आवरण से निकल कर अंततः उसी महान शुद्ध अविनाशी सत् के स्वरुप को प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति की प्राप्ति में प्राणियों के अंदर स्थित अविनाशी सत् विभिन्न शरीरों की यात्रा करता है।
भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि “अविनाशी सत् के स्वरुप की प्राप्ति के लिए अगर तुम नियत कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर की यात्रा जिसका लक्ष्य अपने मूल अविनाशी सत् की प्राप्ति है , सिद्ध नहीं हो सकेगी।” भगवान अर्जुन को इसीलिए बार- बार कह रहे हैं कि “सिर्फ ज्ञानयोग को जान कर उसके प्रति निष्ठा ( अकर्म) से अविनाशी सत् की प्राप्ति नहीं कर पाओगे बल्कि उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा।”
समता की प्राप्ति ही कर्मयोग है :
योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय ।
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥2.48॥
yōgasthaḥ kuru karmāṇi saṅgaṅ tyaktvā dhanañjaya.
siddhyasiddhyōḥ samō bhūtvā samatvaṅ yōga ucyatē৷৷2.48৷৷
अर्थः- “धनंजय! योग में स्थित हो, अपनी आसक्ति को त्याग कर, तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर , तू कर्म कर । इस समता का नाम ही योग है।”
व्याख्याः- भगवान यहां अर्जुन से कह रहे हैं कि “तुम अपनी आसक्ति का त्याग कर दो ।” अर्जुन कई प्रकार की आसक्तियों से ग्रस्त हो चुका है। एक आसक्ति उसे अपने स्वजनों के प्रति है। उसे लगता है कि वो अपने स्वजनों की हत्या कर पाप का भागी होगा।दूसरी आसक्ति जिसकी बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं वो है ‘अकर्म की तरफ उसके प्रेरित हो जाने की’ ।
भगवान ने उसे कहा है कि “जिस सांख्य योग को मैंने तुमसे कहा है, उसके प्रति आसक्त होकर अकर्म में रत मत हो जाना, बल्कि कर्म की तरफ प्रेरित हो जाना।” भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि “ज्ञाननिष्ठा( अकर्म) को छोड़ कर योग ( कर्मयोग) में स्थित हो जाओ। इस योग में स्थित होकर तुम अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए संलग्न हो जाओ।”
कर्म योग का लक्ष्य फल की प्राप्ति नहीं है :
भगवान इस श्लोक से पहले ही कह चुके हैं इस कर्म योग को फल के हेतु मत करो, क्योंकि इस कर्मयोग में ‘आरंभ का नाश नहीं है’। अर्थात् अगर बीच में भी अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए कर्म को छोड़ दोगे तो भी असिद्धि नहीं होगी, बल्कि तुमको इसके परिणाम स्वरुप या फलस्वरुप सत् की ही प्राप्ति होगी । इसलिए अपने कर्म की सिद्धि या असिद्धी के प्रति चिंतित न होकर सिर्फ कर्म कर लो , अविनाशी सत् की प्राप्ति हो जाएगी।
भगवान अर्जुन को सम होने के लिए कहते हैं क्योंकि भगवान ने इसके पहले श्लोक में ही कह दिया है –
यनेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवातो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥2.40॥
nēhābhikramanāśō.sti pratyavāyō na vidyatē.
svalpamapyasya dharmasya trāyatē mahatō bhayāt৷৷2.40৷৷
अर्थः- “यहां( इस कर्मयोग में) आरंभ का नाश नहीं है और प्रत्यवाय( उल्टा फलरुप दोष) भी नहीं है।उसका (कर्मयोग रुपी धर्म का) थोड़ा सा भी अंश बड़े भारी भय से रक्षा कर लेता है।“
व्याख्याः- भगवान अर्जुन को सम होने के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्म योग में न तो आरंभ का नाश है और न ही असफलता में कोई दोष लगता है ,अतः सिद्धि और असिद्धि के भय को त्यागने की बात कह रहे है। भगवान ऐसे ही कर्म को योग कहते हैं, जिसके आरंभ का नाश नही है और असफलता में दोष नहीं है, सिद्धि में भी सत् की प्राप्ति है और असिद्धि में भी अविनाशी सत् की प्राप्ति है। ऐसे कर्म को समभाव से जो भी कर लेता है वो योगी हो जाता है।
सिर्फ बुद्धियोग से संयुक्त कर्म ही श्रेष्ठ हैं :
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥2.49॥
dūrēṇa hyavaraṅ karma buddhiyōgāddhana jaya.
buddhau śaraṇamanviccha kṛpaṇāḥ phalahētavaḥ৷৷2.49৷৷
अर्थः- “हे धनंजय! बुद्धियोग( समत्वरुप बुद्धियोग से संयुक्त कर्म) की अपेक्षा अन्य कर्म अत्यंत तुच्छ हैं।अतः तू बुद्धियोग के ही आश्रय की इच्छा कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन( कृपण, संसारी) होते हैं।”
व्याख्याः- भगवान यहां अर्जुन से कहते हैं कि “बुद्धियोग( कर्मयोग) से किया गया कर्म अविनाशी सत् की प्राप्ति कराता है, जबकि सकाम अर्थात किसी लौकिक, भौतिक फल की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म अत्यंत तुच्छ होता है।”इससे पहले भगवान ने अध्याय 2 के श्लोक 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में अल्पज्ञ और अज्ञानी लोगों के द्वारा बताए गए सकामी वेदोक्त कर्मों के बारे में बता चुके हैं।
राज्य की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति और संतान आदि की प्राप्ति के लिए किए गए सकामी कर्मों का अंत दुखमय ही होता है, क्योंकि इन कर्मों के मूल में अनंत तृष्णा का वास होता है। जबकि सम भाव से सिद्धि और असिद्धि के परवाह किये बिना बुद्धियोग का आश्रय लेकर किया गया कर्म अविनाशी और नित्य शरीरी सत् की प्राप्ति कराता है।
कर्मों में योग ही कुशलता है :
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥2.50॥
buddhiyuktō jahātīha ubhē sukṛtaduṣkṛtē.
tasmādyōgāya yujyasva yōgaḥ karmasu kauśalam৷৷2.50৷৷
अर्थः- “बुद्धियुक्त मनुष्य( समबुद्धि से युक्त मनुष्य) पाप और पुण्य दोनों को यहीं त्याग देता है। अतः तू कर्मयोग के लिए चेष्टा कर , कर्मों में योग ही कुशलता है।”
व्याख्याः- भगवान अर्जुन से कहते हैं कि “समता भाव से युक्त होकर जो कर्म किया जाता है, वो अविनाशी सत् की प्राप्ति कराता है, फिर पाप और पुण्य की बात ही क्या। जब अनंत, अविनाशी और नित्य सत् की प्राप्ति का फल हो तो फिर उसकी सकाम कर्मों के पाप और पुण्य रुपी फल ही प्राप्ति से क्या तुलना हो सकती है?”
- अर्जुन लगातार इस बात पर विषाद कर रहा है कि अपने स्वजनों को मारने से उसे पाप होगा और अगर यह युद्ध धर्मयुक्त भी है तो भी इसे जीत कर जिस पुण्य की प्राप्ति होगी उसे भी उसे नहीं लेना है ।
- भगवान अर्जुन को इसी सकाम युक्त कर्म का त्याग करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तू सकाम कर्मों पर ध्यान ही न दे बल्कि समबुद्धि से युक्त कर्मयोग कर जिससे अविनाशी सत् के स्वरुप का ज्ञान हो सके।
- भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मों में योग ही कुशलता है। अर्थात सिद्धि और असिद्धि के भाव से परे जाकर , पाप और पुण्य के भाव से परे जाकर अपने कर्म का अविनाशी सत् के स्वरुप से योग करा । कर्मों के आचरण में यह बुद्धि का योग ही कौशल है अर्थात अत्यंत सामर्थ्य है। अर्थात् बुद्धियोग बड़ी शक्ति लगाने से ही सिद्ध होता है।
कर्मजनित फल का त्याग जन्मों के बंधन से मुक्त करता है :
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥2.51॥
karmajaṅ buddhiyuktā hi phalaṅ tyaktvā manīṣiṇaḥ.
janmabandhavinirmuktāḥ padaṅ gacchantyanāmayam৷৷2.51৷৷
अर्थातः- “इसलिए कर्मजनित फल का त्याग करके बुद्धियोग से युक्त विवेकी पुरुष जन्मरुप बंधन से मुक्त होकर निरामय पद को प्राप्त कर लेते हैं।”
व्याख्याः- भगवान यहां भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि “सकाम कर्मों का त्याग कर दो और अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले बुद्धियोग का आश्रय लो । इस कर्मयोग को करने से तुम जन्म- मरण के बंधन से मुक्त होकर निरामय पद को प्राप्त कर लोगे।”
- अविनाशी सत् जब त्रिगुणात्मक(सत्व, रज, तम) माया के आवरण में आता है तो वह विभिन्न प्राणियों का शरीर धारण करता है। परंतु प्राणियों के अंदर आवरण में बंद सत् का परम उद्देश्य इस त्रिगुणात्मक शरीर रुपी आवरण के बंधन से मुक्त होकर अविनाशी सत् के रुप में फिर से उसी शुद्ध पद को प्राप्त करना है।
- शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों से होकर गुजरते हुए प्राणी के अंदर स्थित अविनाशी सत् कई जन्मों को धारण करता है अर्थात कई त्रिगुणात्मक आवरण वाले शरीरों को धारण करता है। जिस जन्म में प्राणी को यह ज्ञान हो जाता है कि उसके अंदर अविनाशी सत् है वह इस जन्म जन्मांतर से धारण किए गए त्रिगुणात्मक शरीर रुपी आवरण के बंधन से निकलने के लिए बुद्धियोग के द्वारा प्रयास करता है।
- जिस जन्म में बुद्धियोग द्वारा उसके अंदर स्थित मूल अविनाशी सत् बंधनमुक्त हो जाता है वो निरामय पद यानि असत् रुपी शरीर के जन्म बंधन चक्र से मुक्त होकर शुद्ध अविनाशी सत् के रुप में मुक्त हो जाता है।
श्रीमद्भगवद्गीता में मोह का त्याग और वैराग्य का ज्ञान :
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥2.52॥
yadā tē mōhakalilaṅ buddhirvyatitariṣyati.
tadā gantāsi nirvēdaṅ śrōtavyasya śrutasya ca৷৷2.52৷৷
अर्थः- “जब तेरी बुद्धि मोह रुपी कीचड़ या दलदल को पार कर जाएगी, तब तू पहले सुने हुए और भविष्य में सुनने में आने वाले फलों या भोग से वैराग्य प्राप्त कर लोगे।”
व्याख्याः- भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि “तेरी बुद्धि अभी कर्म योग से युक्त नहीं हुई है और तू अभी भी सकामी कर्मों के चक्कर में ही फंसा हुआ है । सकामी कर्म व्यक्ति मे मोह, लोभ, क्रोध आदि उत्पन्न करते हैं।”
- सकामी मनुष्य कोई भी कर्म किसी फल प्राप्ति के लिए करता है। भगवान ने पहले भी कहा है कि अल्पज्ञ और अज्ञानी जन वेदों के मूल अर्थ को जाने बिना उसके बाहरी अर्थों की व्य़ाख्या करते हैं और कहते रहे हैं कि इस यज्ञ को करने से या फिर इस मंत्र के जाप से राज्य, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है।
- भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अल्पज्ञ और अज्ञानी लोग कहते हैं कि अमुक कर्म को करने से मनुष्य पाप का भागी होगा । तू भी इन पहले से सुने हुए और भविष्य में प्राप्त होने वाले फलों को लेकर मोह ग्रस्त है।तूझे लगता है कि अगर तूने भीष्म आदि स्वजनों को मार दिया तो तू पाप का भागी हो जाएगा ।
- भगवान कहते हैं कि ऐसे पहले से सुनने में अल्पज्ञ और अज्ञानी लोगों की बातों और भविष्य में भीष्म आदि की संभावित हत्या से उत्पन्न पाप के भागी होने के मोह और डर से जब तू मुक्त हो जाएगा तब तेरा इन बातों से वैराग्य हो जाएगा।
राग, विराग और वैराग्य क्या हैं?
शास्त्रों में राग, विराग और वैराग्य की बातें कही गई हैं। राग अर्थात मोह से उत्पन्न आसक्ति। विराग अर्थात किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति नफरत । लेकिन भगवान अर्जुन को राग और विराग दोनों से ही परे जाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वैराग्य राग और विराग दोनों से परे और दोनों की ही सम स्थिति है। वैराग्य एक दम बीच की स्थिति है । न तो किसी से आसक्ति और न ही किसी के प्रति विरक्ति।
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥2.53॥
śrutivipratipannā tē yadā sthāsyati niścalā.
samādhāvacalā buddhistadā yōgamavāpsyasi৷৷2.53৷৷
अर्थः- “मेरे द्वारा सुने गए उपदेश से भली भांति प्रपन्न हुई तेरी बुद्धि जब अचल होकर मन (यानि समाधि) में निश्चल भाव से ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा।”
व्याख्याः- भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं जिस बुद्धियोग के बारे में तुझे ज्ञान दे रहा हूं अगर तू उसे ठीक से सुनेगा तब तेरी बुद्धि अचल हो जाएगी और तू योग अर्थात बुद्धियोग को प्राप्त हो जाएगा । अभी तक भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अल्पज्ञ और अज्ञानी लोगों के द्वारा बताए गए पाप – पुण्य फल रुपी सकामी कर्मों का जब तू त्याग कर देगा तब तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जब तू इन मोह रुपी द्वंद्वों( पाप- पुण्य, लाभ- हानि, जय-पराजय) से उपर उठ जाएगा तब तेरा मन स्थिर और अचल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ही तू कर्म योग करने वाले ज्ञान को समझ सकेगा और उस योग को करने के लिए तत्पर होगा ।
और पढ़िए :