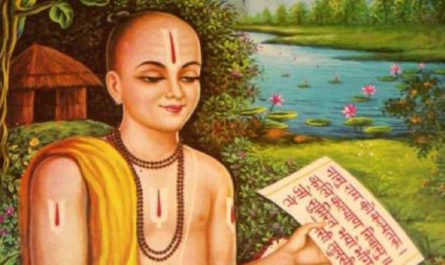अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण और कर्म को भगवान ने अध्याय 3 के श्लोक 17 से 24 में अर्जुन को बताया कि अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए आसक्तिरहित यज्ञकर्म करने की आवश्यकता है। आसक्तिरहित यज्ञकर्म करना न केवल स्वयं के लिए आवश्यक है, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी जरुरी है। भगवान ने यह भी कहा कि हालांकि उनके लिए कोई भी कर्म करना आवश्यक नहीं है, फिर भी वो लोकसंग्रह के लिए कर्म करते हैं, ताकि दूसरे लोग उनका आचरण कर धर्मानुसार समाज की स्थापना में संलग्न रहें और समाज सुव्यवस्थित रहे ।
अज्ञानी और ज्ञानवान कौन है?
अब भगवान अर्जुन को ज्ञानी और अज्ञानी के लक्षण तथा उसके कर्म बताने जा रहे हैं –
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥
saktāḥ karmaṇyavidvāṅsō yathā kurvanti bhārata.
kuryādvidvāṅstathāsaktaśicakīrṣurlōkasaṅgraham৷৷3.25৷৷
अर्थः- हे भारत कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग जिस प्रकार के कर्म करते हैं , वैसे ही विद्वान को अनासक्त होकर लोकसंग्रह ( लोगों की भलाई ) के लिए कर्म करना चाहिए।
व्याख्याः- भगवान ने पिछले श्लोकों में अर्जुन को यह बताया था कि ज्ञानयोग (अविनाशी सत् के तत्व को जान कर ) के अधिकारी होने के बाद भी आत्मसाक्षात्कार के लिए अविनाशी सत् की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले यज्ञकर्म को जरुर करना चाहिए ।
इससे उस पुरुष की भी मुक्ति होती है और साथ में वो अपने श्रेष्ठ आचरण कर्म के द्वारा लोगों को प्रेरित भी कर सकता है अर्थात् लोकसंग्रह कर सकता है।
अज्ञानी भी प्रेरित होकर अच्छे कर्म कर सकते हैं
भगवान कहते हैं कि सिर्फ ज्ञानयोग को जानने वाले ही यज्ञकर्म नहीं करते, बल्कि श्रेष्ठ पुरुषों से प्रेरित होकर अज्ञानी लोग भी अच्छे कर्म करने लगते हैं। अज्ञानी अपने अच्छे कर्म श्रेष्ठ पुरुषों की प्रेरणा में आकर करते तो हैं , लेकिन उनके अंदर ज्ञानयोग के अभाव की वजह से फल प्राप्ति की इच्छा का भाव होता है। ऐसे अज्ञानी लोग भी कर्मकांडीय यज्ञ करते हैं ताकि उन्हें संतान, सुख, राज्य आदि की उपलब्धि हो सके। ऐसे लोग कर्म और उसके फल के प्रति आसक्त रहते हैं। भगवान कहते हैं कि उपरी तौर पर कर्म में आसक्त लोगों के कर्मों और ज्ञानयोग से लब्ध आसक्तिरहित पुरुषों के कर्म में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। लेकिन, एक फर्क यही होता है कि ज्ञानयोग से लब्ध पुरुष के द्वारा किए जाने वाले कर्म में फल की आकांक्षा नहीं होती है, वो सिर्फ अविनाशी सत् की प्राप्ति हेतु एवं लोगों की भलाई (लोकसंग्रह) हेतु यज्ञकर्म करता है।
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङि्गनाम् ।
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥
na buddhibhēdaṅ janayēdajñānāṅ karmasaṅginām.
jōṣayētsarvakarmāṇi vidvān yuktaḥ samācaran৷৷3.26৷৷
अर्थः- विद्वान पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे बल्कि योगयुक्त कर्म करते हुए सभी कर्मों में उनकी प्रीति उत्पन्न करे (यानी सभी कर्म प्रेमपूर्वक कराए) ।
व्याख्याः- भगवान यहां विद्वान पुरुष से आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न कराने के लिए आग्रह कर रहे हैं। विद्वान कौन है ? शास्त्रों में क्रियावान पुरुष को ‘विद्वान’ कहते हैं। भगवान यहां ‘योगयुक्त’ कर्म करने के लिए भी कह रहे हैं।
‘योगयुक्त’ कौन है? भगवान योगयुक्त पुरुष की परिभाषा गीता के अध्याय 6 के श्लोक 8 में देते हैं –
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः।।6.8।।
अर्थः- जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेन्द्रिय है, और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धिवाला है, ऐसा योगीयुक्त (योगारूढ़) कहा जाता है।
भगवान कहते हैं कि जो क्रियावान (विद्वान) और ‘योगयुक्त’ पुरुष है अर्थात जो ज्ञानयोग के साधन में समर्थ है, उसे भी चाहिए कि जो लोग अविनाशी सत् के तत्व को समझने में असमर्थ हैं, या अज्ञानी हैं , और सकाम कर्म करने में ही लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि को भ्रमित न करें।
अपना उदाहरण पेश करें :
भगवान विद्वान और योगयुक्त पुरुष को ऐसा न करने के लिए इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि अज्ञानी तो फल की इच्छा से ही सही अच्छा कर्म तो प्रारंभ करे । अज्ञानी किसी ज्ञानयोग लब्ध पुरुष की प्रेरणा से आकर संतान, सुख, संपत्ति, राज्य आदि के लिए ही सही कर्मकांडीय यज्ञों, पूजा- पाठ आदि के द्वारा कुछ तो कर्म करने के लिए प्रेरित हुआ है। यदि ऐसे सकामी अज्ञानी पुरुष के बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा हो जाए और वो ऐसे सकामी कर्मों का भी त्याग कर दें तो उनका तो नाश ही हो जाएगा।
ज्ञानी को तो न केवल सिर्फ स्वयं अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए समत्व बुद्धि से युक्त होकर यज्ञकर्म करना है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अपने उस समत्व बुद्धि युक्त कर्म का उदाहरण पेश कर अज्ञानियों के मन और बुद्धि के अंदर अविनाशी सत् की प्राप्ति हेतु प्रेरणा उत्पन्न करना भी है ।
प्रकृति के गुण क्या हैं :
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥
prakṛtēḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ.
ahaṅkāravimūḍhātmā kartā.hamiti manyatē৷৷3.27৷৷
अर्थः-कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों के द्वारा किये जाते हैं, परंतु अहंकार से मूढ़ात्मा (मोहित अंतःकरण वाला) ‘मैं कर्ता हूं’ ऐसा मान लेता है।
व्याख्याः- पुरुष का शरीर तीन प्राकृतिक गुणों से बना होता है । गीता के अध्याय 14 के 5वें श्लोक में भगवान प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों के बारे में कहते हैं जो अविनाशी सत् को एक शरीर में बांध लेते है –
‘सत्वगुण’ किसे कहते हैं?
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः।
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्।।14.5।।
अर्थः- हे महाबाहो ! प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले सत्त्व, रज और तम — ये तीनों गुण अविनाशी देहीको देह में बाँध देते हैं।
इसके बाद अध्याय 14 के श्लोक 6 में भगवान ‘सत्वगुण’ की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि –
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्।
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ।।14.6।।
अर्थः- हे पापरहित अर्जुन ! उन गुणों में ‘सत्त्वगुण’ निर्मल (स्वच्छ) होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से (देहीको) बाँधता है। अर्थात् ‘सत्वगुण’ किसी भी विकार से रहित है।
‘सत्वगुण’ सुख और ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है और अविनाशी सत् को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है और उसे सुख और ज्ञान की प्राप्ति की तरफ प्रेरित करता है। शरीर के अंदर स्थित अविनाशी सत् को वह ईश्वर रुपी परम अविनाशी सत् की तरफ प्रेरित और प्रकाशित करता है, इसलिए ‘सत्वगुण’ निर्मल है।
रजोगुण क्या है : गीता के अध्याय 14 के श्लोक 7 में भगवान अर्जुन को ‘रजोगुण’ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि –
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्।
तन्निबध्ना ति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्।।14.7।।
अर्थः- हे कुन्तीनन्दन ! तृष्णा और आसक्ति को पैदा करनेवाले ‘रजोगुण’ को तुम रागस्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बाँधता है। भगवान ‘रजोगुण’ की जिस विशेषता को बता रहे हैं वह ‘तृष्णा’ और ‘आसक्ति’ को पैदा करता है । ‘रजोगुण’ किसी पुरुष के अंदर संसार के प्रति अनुराग से भर देता है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि तृष्णा सभी दुःखों का मूल है।
तमोगुण किसे कहते हैं: इसके बाद गीता के अध्याय 14 के ही श्लोक 8 में भगवान ‘तमोगुण’ की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि –
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्।
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत।।14.8।।
अर्थः- हे भरतवंशी अर्जुन ! सम्पूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले ‘तमोगुण’ को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देहधारियों को बाँधता है।
यहां भगवान ‘तमोगुण’ की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि यह अज्ञान या अविद्या से उत्पन्न होता है और अविनाशी सत् को धारण करने वाले शरीर को मोह से युक्त कर देता है। इसके अलावा वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देहधारी ( अविनाशी सत् ) को परमेश्वर ( अविनाशी सत् के वृहदत्तम अँश) से दूर कर देता है। जहां ‘सत्वगुण’, सुख और ज्ञान के प्रति आसक्त करता है वहीं ‘रजोगुण’, तृष्णा और राग के प्रति आसक्त कर देता है और ‘तमोगुण’ अज्ञान और आलस्य के प्रति अविनाशी सत् धारी शरीर को आसक्त कर देता है।
त्रैगुणात्मक प्रकृति अंहकार को जन्म देती है
सत्व, रज और तमो तीनों ही गुण आसक्ति युक्त हैं , जबकि भगवान समत्व बुद्धि से युक्त होकर आसक्ति रहित हो कर अविनाशी सत् की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले यज्ञ कर्म को करने के लिए कहते हैं। भगवान यह भी कहते हैं कि अविनाशी सत् को जब प्रकृति के तीनों गुण एक शरीर से बांध देते हैं तो अंतःकरण में ‘अहंकार’ का जन्म होता है। ‘अहंकार’ से ही आसक्ति उत्पन्न होती है। अहंकार से ही ‘मैं’ रुपी ‘नाम- रुप’ की अभिव्यक्ति होती है। आसक्ति से भरे अहंकार युक्त शरीर को यह भ्रम हो जाता है कि जो कर्म वह कर रहा है वो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न नहीं है , बल्कि वही इसका कर्ता है।
फिर, अहंकार और आसक्ति से युक्त शरीर अगर फल की प्राप्ति के लिए कर्मकांडीय यज्ञ को भी करता है, तो उसके अंदर यही भाव होता है कि उस कर्म का कर्ता वही है। जबकि वास्तविक यज्ञकर्म वही है जो तीनों प्रकृति के गुणों से उत्पन्न विकार से रहित और अहंकार से रहित होकर अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
त्रैगुणात्मक गुणों के प्रति आसक्ति से बचें
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥
tattvavittu mahābāhō guṇakarmavibhāgayōḥ.
guṇā guṇēṣu vartanta iti matvā na sajjatē৷৷3.28৷৷
अर्थः- परंतु हे श्रेष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन गुण-कर्म- विभाग के तत्त्व को जानने वाला ‘गुण ही गुणों में बरत रहे हैं’ ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता ।
व्याख्याः- भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो गुण- कर्म के विभाग के तत्व को जानता है, उसे इस बात का ज्ञान होता है, कि अविनाशी सत् किसी भी गुण और कर्मों से परे और निर्मल है।
जो सत्व, रज और तम के गुणों और उनसे उत्पन्न कर्मों के प्रकारों और विभागों को जान लेता है, वो यह भी जान लेता है कि ये सारे सासांरिक कर्म इन्हीं से उत्पन्न हैं, और इस त्रैगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न शरीर और उसकी इंद्रियों और चेष्टाओं से ही सांसारिक कर्मों की उत्पत्ति होती है, जो इसी प्रकृति से उत्पन्न जड़ और चेतन पदार्थों की प्राप्ति हेतु कर्म करती है। अविनाशी सत् किसी भी कर्म में लिप्त ही नहीं होता । ऐसे ज्ञान को जान लेने वाला कभी भी आसक्त नहीं होता ।
गुण-विभाग और कर्म-विभाग क्या हैं?
- सत्व, रज और तम इन तीन गुणों को धारण करने वाली त्रैगुणात्मक प्रकृति से पांच जड़ महाभूत( पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु) उत्पन्न होते हैं, और इसी त्रैगुणात्मक प्रकृति से मन, बुद्धि , अहंकार नामक चेतनाएं उत्पन्न होती है।
- इसी त्रैगुणात्मक प्रकृति से शरीर की पांच इंद्रियां( श्रोत्र, जिव्हा, चक्षु, घ्राणेंद्रिय या कान और त्वचा) भी निर्मित होती है। इसके अलावा पांच कर्मेंद्रियां ( वाक्, हाथ, पैर, गुदा और लिंग) और पांच विषय( शब्द,रुप, रस, गंध और स्पर्श) भी उत्पन्न होते हैं।
- त्रैगुणात्मक प्रकृति( सत्व, रज और तम) से उत्पन्न इस समूह या समुदाय का नाम ‘गुण- विभाग’ है। इन ‘गुण-विभाग’ द्वारा किए गए कर्मों या चेष्टाओं का नाम ‘कर्म- विभाग’ है।
- उदाहरण के लिए त्वचा में स्पर्श का गुण होता है। जब हम अपने हाथ रुपी कर्मेंद्रिय में स्थित त्वचा रुपी इंद्रिय को अग्नि रुपी महाभूत के पास ले जाने का कर्म करते हैं, तो हमारे मन रुपी चेतना को को स्पर्श रुपी विषय होता है, इससे हमारी त्वचा को अग्नि के दाह का अनुभव होता है और हमारी बुद्धि उस हाथ को अग्नि से दूर ले जाती है।
- भगवान कहते हैं कि ये सारे कर्म त्रैगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न गुण-कर्म विभागों के द्वारा किये जाते हैं, न कि त्रैगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न शरीर के अंदर स्थित अविनाशी सत् के द्वारा किए जाते हैं । जो इस रहस्य को जान लेता है वो इन कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता है।
प्रकृति से मोहित मनुष्य आसक्त हो जाता है
प्रकृतेर्गुणसम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥
prakṛtērguṇasammūḍhāḥ sajjantē guṇakarmasu.
tānakṛtsnavidō mandānkṛtsnavinna vicālayēt৷৷3.29৷৷
अर्थः- प्रकृति के गुणों से मोहित (यानि मूढ़ हुए मनुष्य) गुण-कर्मों में आसक्त होते हैं। पूर्ण जानने वाला ( ज्ञानी) उस अल्पज्ञ या मंदबुद्धि को चलायमान न करे।
व्याख्याः- भगवान इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि जो ज्ञानयोग से लब्ध है अर्थात जिसने यह जान लिया है कि अविनाशी सत् किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता, और जो भी कर्म हमें दिखते हैं वो त्रैगुणात्मक प्रकृति के गुण-कर्मों के विभाग से उत्पन्न होते हैं, वह फिर किसी कर्म में आसक्त नहीं होता ।
लेकिन, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो किसी प्रकार का कर्म नहीं करता । वह ज्ञानी भी आत्मसाक्षात्कार के लिए यज्ञरुपी( अविनाशी सत् की प्राप्ति ) कर्म करता रहता है । साथ में वह ज्ञानी सांसारिक कर्मों को भी करता रहता है ताकि शरीर धर्म की भी रक्षा हो सके। इसके अलावा ज्ञानी उन कर्मों को भी करता है जो फलरुपी कर्मकांडीय यज्ञों के रुप में किये जाते हैं।
भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है वह लगातार इन सारे वेदविहित कर्मकांडीय कर्मों को करता रहे, ताकि लोक संग्रह के लिए वे कर्म अल्पज्ञों के लिए भी उदाहरण बन सकें, और अल्पज्ञ और मंदबुद्धि भले ही ज्ञानयोग के लिए किये जाने वाले यज्ञकर्मों के तत्त्व को न जानते हों, लेकिन वो फलरुपी कर्मकांडीय यज्ञों को तो करते रहें।
भगवान की चेतावनी
- भगवान यहां ज्ञानयोग से लब्ध और अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए यज्ञकर्म करने वाले पुरुष को चेतावनी भी देते हैं, कि अगर तुमने सांसारिक कर्मों और विशेषकर फलरुपी कर्मों को त्याग दिया, तो तुमसे प्रेरित होकर ये मंदबुद्धि भी इन कर्मों को करना बंद कर देंगे। इसलिए इन मंदबुद्धियों को ज्ञानी पुरुष भटकने न दे।
- कम से कम ये अल्पज्ञ और मंदबुद्धि वाले पुरुष अविनाशी तत्त्व को जाने बिना ही सही, और फलरुप कर्मकांडीय यज्ञों के द्वारा ही सही किसी न किसी सात्विक कर्म की तरफ प्रेरित तो हो ही रहे हैं । सात्विक कर्म उनकी बुद्धि को निर्मल करेगा और ज्ञान की तरफ आसक्त करेगा। एक बार ज्ञान की तरफ आसक्ति हो जाएगी तो हो सकता है भविष्य में वो आसक्ति रहित यज्ञकर्म कर सकें और अविनाशी सत् की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकें।
- लेकिन, अगर ज्ञान लब्ध पुरुष ने अपना यज्ञकर्म और अन्य सांसारिक फल प्राप्ति हेतु किये जाने वाले सात्विक कर्मों का त्याग कर दिया तो फिर इन मंदबुद्धियों का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा।
अध्यात्म चित्त क्या है?
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नयस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥
mayi sarvāṇi karmāṇi saṅnyasyādhyātmacētasā.
nirāśīrnirmamō bhūtvā yudhyasva vigatajvaraḥ৷৷3.30৷৷
अर्थः- अध्यात्म चित्त से सब कर्मों को मुझे निक्षेप करके (यानी मुझको सौंप कर) आशा, ममता,संताप से रहित होकर युद्ध कर।
व्याख्याः- भगवान स्वयं अविनाशी सत् के वृहदत्तम अँश हैं और सभी प्राणियों की अंतरात्मा में स्थित हैं, स्वयं भगवान ने गीता के अध्याय 18 के श्लोक 61 में कहा है –
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।।18.61।।
अर्थः-हे अर्जुन ! ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीररूपी यन्त्र पर आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियों को (उनके स्वभावके अनुसार) भ्रमण कराता रहता है। अर्थात् ईश्वर अपनी त्रैगुणात्मक माया से किसी प्राणी के शरीर को सृजित करता है और अविनाशी सत् के लघु अँश को उसके हद्य में स्थित कर देता है।
इस अविनाशी सत् के लघु अँश को वो त्रैगुणात्मक माया से बनाए गए शरीर रुपी यंत्र के जरिए इस संसार में विभिन्न कर्मों के द्वारा भ्रमण कराता रहता है। यहां भ्रमण कराने से तात्पर्य अविनाशी सत् के लघु अँश को त्रैगुणात्मक प्रकृति से सृजित शरीर के द्वारा उसे त्रैगुणात्मक प्रकृति या माया से ही उत्पन्न जड़ और चेतन पदार्थों से निर्मित संसार में भटकाते रहना है।
भगवान अर्जुन को अब इस त्रैगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न संसार और सांसारिक कर्मों से अविनाशी सत् को मुक्त कराने का उपाय बता रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम पहले अध्यात्म चित्त हो जाओ। आत्म विषयक चेतना को ही ‘अध्यात्म चित्त’ होना कहते हैं। जब पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि उसके अंदर स्थित अविनाशी सत् उसी परमेश्वर रुपी अविनाशी सत् का अंग है तो वो इस ज्ञान को प्राप्त कर बाहरी जगत से अपने चित्त को मोड़ कर अपने अंदर स्थित अविनाशी सत् की तरफ लगा देता है। इसे ही अध्यात्म चित्त होना कहा गया है।
अविनाशी सत् रुपी ईश्वर के प्रति समर्पण
- भगवान कहते हैं कि पहले तू अध्यात्म चित्त हो जा और इसके बाद जब तुझे यह ज्ञान हो जाएगा कि त्रैगुणात्मक माया से बने इस शरीर के अंदर स्थित अविनाशी सत् का लघु अँश वास्तव में अविनाशी के वृहदत्तम अँश का ही एक अंग है, तब तू अपने समस्त कर्मों को उसी मुझ परमेश्वर रुपी अविनाशी सत् की तरफ लगा देगा ।
- ऐसी स्थिति में तू समस्त कर्मो को अविनाशी सत् की तरफ ही लगा कर आशा, ममता, और संताप जैसे विषयों से मुक्त होकर युद्ध को यज्ञकर्म मान कर करेगा।
- भगवान कहते हैं कि तू युद्धकर्म को यज्ञकर्म बना ले और इस हिंसक युद्ध को भी यज्ञकर्म मान कर उसे अविनाशी सत् की प्राप्ति की तरफ लगा दे। सिर्फ युद्धकर्म ही नहीं बल्कि समस्त कर्मों( चाहे वो फल प्राप्ति हेतु शास्त्रोक्त कर्मकांडीय कर्म हों या सांसारिक कर्म हों) को अध्यात्म चित्त होकर मुझ अविनाशी सत् की प्राप्ति हेतु समर्पण भाव से लगा दे ।
- भगवान जानते हैं कि अर्जुन अपने स्वजनों के प्रति ममता के भाव से ग्रस्त है, इस आशा से वह युद्ध नहीं करना चाहता कि शायद उसके युद्ध न करने से उसके स्वजनों के प्राण बच जाएंगे। वह इस संताप से भी ग्रस्त है, कि अगर युद्ध में उसके स्वजन मारे जाएंगे तो उसके कुल का धर्म भी नष्ट हो जाएगा।
- भगवान इसी लिए अर्जुन को कर्ता के भाव से मुक्त करने का उपाय बताते हैं, और कहते हैं कि तू यह जान ले कि तेरे त्रैगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न शरीर के भीतर मैं ही अविनाशी सत् के रुप में विद्यमान हूं। इसलिए अगर तू अपने कर्मों को मुझ अविनाशी सत् के प्रति समर्पित कर देगा तो तू इस संताप से भी मुक्त हो जाएगा कि युद्ध कर्म से पाप की प्राप्ति होगी।
ईश्वर का मत ही श्रेष्ठ है
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽति कर्मभिः ॥
yē mē matamidaṅ nityamanutiṣṭhanti mānavāḥ.
sraddhāvantō.nasūyantō mucyantē tē.pi karmabhiḥ৷৷3.31৷৷
अर्थः- जो मनुष्य दोष न देखते हुए , श्रद्धा रखते हुए मेरे इस मत का सदा अनुष्ठान( अनुसरण) करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
व्याख्याः- भगवान ने अर्जुन को समत्व बुद्धि से आसक्ति रहित होकर युद्ध रुपी कर्म को यज्ञकर्म मान कर अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए कर्म करने के कहा।
अब भगवान कहते हैं कि जो लोग ऐसे यज्ञकर्म को तो नहीं कर सकते लेकिन कम से कम इस मत का अनुसरण कर सांसारिक कर्मों को भी सात्विक भाव से करते हैं, वो ज्ञान और मुक्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं। सात्विक भाव के जागने से उनका अंतर्मन प्रकाशमान हो सकता है। और हो सकता है कि वो भविष्य में अविनाशी सत् की प्राप्ति हेतु यज्ञकर्म करने लगें। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानलब्ध होकर अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए यज्ञकर्म कर रहा है, वो तो कर्मबंधनों से मुक्त हो ही जाएगा। लेकिन, जो इस मत की निंदा न करके इस मत पर श्रद्धा भी रख रहा है तो भविष्य में उसके भी अविनाशी सत् को प्राप्त करने और कर्म बंधनों से मुक्त होने की संभावना निश्चित है।
श्रद्धा और अनसूया भाव किसे कहते हैं?
‘श्रद्धा’ का अर्थ होता है ‘जिस कर्म से सत्य वस्तु को धारण किया जाए’ अर्थात वेदों और श्रुतियों में ईश्वर विषयक या अविनाशी सत् से संबंधित बताए गए मतों को धारण किया जाए। जो भी ऐसा करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है और अविनाशी सत् को प्राप्त कर सकता है।
भगवान ने ‘श्रद्धा’ के साथ साथ ‘अनसूया’ की भी बात कही है। ‘अनसूया’ के विषय में कहा जाता है कि जो किसी गुणवान के गुणों का खंडन नहीं करता, थोड़े गुणों वाले की भी प्रंशसा करता है और दूसरों के दोष नहीं देखता, मनुष्य का वह भाव ‘अनसूया’ कहलाता है। भगवान यह भी कहते हैं कि जिसने सत्य को धारण कर अविनाशी सत् संबंधी मत के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं किया है लेकिन कम से कम उसकी निंदा भी नहीं करता और उसमें दोष नहीं देखता अर्थात् अनसूया भाव को उपलब्ध होता है, उसके भी भविष्य में कर्मबंधन से मुक्त होने की संभावना निश्चित है।
ईश्वर के मत में दोष निकालने वाले मूर्ख होते हैं
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥
yē tvētadabhyasūyantō nānutiṣṭhanti mē matam.
sarvajñānavimūḍhāṅstānviddhi naṣṭānacētasaḥ৷৷3.32৷৷
अर्थः- परंतु जो मेरे इस मत को दोष- दृष्टि से देखते हुए (अर्थात दोष निकालते हुए) उसका अनुष्ठान या अनुसरण नहीं करते उसको तू सर्वज्ञान से मूढ़(घोर मूर्ख) , चेतना रहित और नष्ट समझो।
व्याख्याः- भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस मत ( अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञकर्म से मुक्ति का सिद्धांत) को दोष-दृष्टि से देखते हैं अर्थात इस सिद्धांत को गलत मानते हैं और इसमें श्रद्धा नहीं रखते या अनुसरण नहीं करते वो सर्वज्ञान ( अविनाशी सत् के बारे में ज्ञान ) से रहित होते हैं।
भगवान ने ‘श्रद्धावान’ की परिभाषा देते हुए गीता के अध्याय 4 के 39वें श्लोक में कहा है –
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।।4.39।।
अर्थः-जो जितेन्द्रिय तथा साधन-परायण है, ऐसा श्रद्धावान् मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है।
अर्थात् जिसकी अविनाशी परमेश्वर के मत के प्रति श्रद्धा है ,वो आज नहीं तो कल ज्ञानलब्ध हो ही जाएगा और अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए कर्मयोग या यज्ञकर्म में लग जाएगा। लेकिन जो इस ‘सर्वज्ञान’ जो कि सृष्टि का मूल ज्ञान है उसमें दोष निकालता है , वो तो मूर्ख हैं ही साथ ही चेतना रहित भी है। जो अविनाशी सत् के यथार्थ ज्ञान को समझ लेता है वही ‘चेतनावान’ है। लेकिन जो सांसारिक लोभ- मोह. जय-पराजय आदि में लिप्त रहता है वो इस ज्ञान को झूठा समझता है इसलिए उसके अंदर अविनाशी सत् के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या उसका अनुसरण करने के लिए चेतना उत्पन्न नहीं होती ।
मूर्ख ही बार- बार जन्म लेता है
ऐसा मूर्ख और चेतना रहित व्यक्ति सांसारिक कार्यों में ही लिप्त रहता है और शरीर को ही सब कुछ समझते हुए मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे शरीरों के रुप में जन्म लेता रहता है । वह इस संसार चक्र से मुक्त नहीं हो पाता । भगवान ने यही बात गीता के अध्याय 16 के 20 वें श्लोक में भी कही है –
असुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि।
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्।।16.20।।
अर्थः-हे कुन्तीनन्दन ! वे मूढ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके ही जन्म-जन्मान्तर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में चले जाते हैं।
ज्ञानी भी सांसारिक कर्म करते हैं
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥
sadṛśaṅ cēṣṭatē svasyāḥ prakṛtērjñānavānapi.
prakṛtiṅ yānti bhūtāni nigrahaḥ kiṅ kariṣyati৷৷3.33৷৷
अर्थः-ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति (पूर्व वासना) के सदृश चेष्टा करता है। सभी प्राणी प्रकृति की ओर जा रहे हैं तो फिर निग्रह क्या करेगा ?
व्याख्याः- भगवान कहते हैं कि सांसारिक कर्मों से कोई भी बच नहीं सकता है। जो अविनाशी सत् को जान लेता है और उसकी प्राप्ति के लिए कर्मयोग या यज्ञकर्म करता है, वो भी सांसारिक कर्म करता ही है।
- भगवान कहते हैं कि त्रैगुणात्मक प्रकृति (सत्व, रज, तम) से उत्पन्न पंच महाभूत( पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश) और गुण-कर्म से उत्पन्न शरीर अपनी इंद्रियों और उससे उत्पन्न विषयों से ज्ञानी भी नहीं बच सकता।
- शरीर के निर्वाह के लिए इंद्रियों से जनित कर्म कर्म करने ही पड़ते हैं। सभी प्राणी त्रैगुणात्मक प्रकृति के प्रभाव की तरफ उन्मुख होते ही हैं। जब अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए भी शरीर आवश्यक है तो फिर शरीर के निर्वाह के लिए सांसारिक कर्मों को करने से कोई बच नहीं सकता और न ही कोई इसका निग्रह कर सकता है। इसलिए भगवान ज्ञानी को सांसारिक कर्मों से विमुख होने की सलाह नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि इनको करते हुए भी अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए कर्मयोग करते रहो।
- हां ! शरीर निर्वाह के लिए सांसारिक और इंद्रिय जनित कर्मों को करते हुए भी, अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए यज्ञकर्म करते रहना चाहिए। ताकि शरीर निर्वाह के साथ- साथ अविनाशी सत् की प्राप्ति कर मुक्ति भी प्राप्त की जा सके ।
राग-द्वेष सबसे बड़े शत्रु हैं
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥
indriyasyēndriyasyārthē rāgadvēṣau vyavasthitau.
tayōrna vaśamāgacchēttau hyasya paripanthinau৷৷3.34৷৷
अर्थः- इंद्रिय- इंद्रिय के विषय में (यानी समस्त इंद्रियों के भोगों में) जो राग-द्वेष स्थित है,उनके वश में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही पुरुष के मार्ग को रोकने वाले हैं।
व्याख्याः- भगवान ने यहां दो बार इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। भगवान कहते है कि त्रैगुणात्मक प्रकृति के प्रभाव से इन दोनों ही इंद्रिय प्रकारों में राग और द्वेष नामक भाव स्थित होते हैं।
राग में आकर ही हम किसी कर्म को करने के लिए मोहित और आकर्षित होते हैं। इंद्रियों के कर्मों को बलपूर्वक रोकने से हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में क्रोध आदि द्वेष भावों का उदय होता है। भगवान कहते हैं कि सांसारिक कर्म करना शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है। इंद्रिय और उसके विषयों को पूरा करने के दौरान राग-द्वेष नामक शत्रु आते ही हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को इनसे उत्पन्न होने वाले कर्मों को तो करना चाहिए लेकिन इनका दास नहीं बनना चाहिए और इसके वश में नहीं आना चाहिए। क्योंकि यही राग और द्वेष अविनाशी सत् की प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं। मनुष्य राग और द्वेष में आकर ही शरीर को कर्ता मान लेता है।
किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए?
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥
śrēyānsvadharmō viguṇaḥ paradharmātsvanuṣṭhitāt.
svadharmē nidhanaṅ śrēyaḥ paradharmō bhayāvahaḥ৷৷3.35৷৷
अर्थः- अच्छी तरह से अनुष्ठान किये हुए पराये धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी श्रेष्ठ है, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, परंतु पराया धर्म भयावह है।
व्याख्याः- भगवान ने यही बात गीता के अध्याय 18 के 47वें श्लोक में भी कही है-
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।।18.47।।
अर्थः-अच्छी तरह से अनुष्ठान किये हुए परधर्म से गुणरहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। कारण कि स्वभाव से नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता।
स्वधर्म और परधर्म क्या हैं?
‘स्वधर्म’ वह है जो अविनाशी सत् के वृहदत्तम अँश ईश्वर के प्रति किया जाए। यहां ‘धर्म’ विष्णुवाचक होने की वजह से ईश्वर के प्रति किया जाने वाला कर्म हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ‘स्वधर्म’ यानि अविनाशी सत् स्वरुप ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञकर्म रुपी धर्म श्रेष्ठ है। अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले धर्म रुपी यज्ञकर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है क्योंकि इस मृत्यु से मुक्ति या मोक्ष मिल जाता है।
‘स्वधर्म’ गुणरहित है और ‘परधर्म’ गुणयुक्त है
- भगवान ‘स्वधर्म’ को ‘गुणरहित’ बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अविनाशी सत् त्रैगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न गुणों से मुक्त होता है और इससे परे होता है। इसलिए ‘स्वधर्म’ गुणरहित है। जो त्रैगुणात्मक माया रुपी गुणों से परे है वो तो अविनाशी सत् ही है और उससे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता है।
- लेकिन ‘परधर्म’ अर्थात शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म ‘गुणयुक्त’ होता है, क्योंकि वह त्रैगुणात्मक प्रकृति(सत्व, रज और तम) गुणों से युक्त होता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे परधर्म अर्थात अविनाशी सत् की प्राप्ति के लिए किये गए स्वधर्म के अतिरिक्त जो भी कर्म हैं, वो परधर्म हैं ।
- अगर ‘धर्म’ विष्णु वाचक है तो ‘परधर्म’ वह कर्म है, जो अविनाशी सत् के वृहदत्तम साकार विष्णु स्वरुप की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा रहा हो। जो अविनाशी सत् के प्रति किया जाने वाला कर्म नहीं है वो ‘परधर्म’ या सांसारिक त्रैगुणात्मक कर्म है।
भगवान पहले ही कह चुके हैं जो अविनाशी सत् के प्रति किये जाने वाले कर्म(स्वधर्म) के प्रति श्रद्धा नहीं रखता और उसमें दोष देखते हुए केवल शरीर निर्वाह के लिए सांसारिक कर्मों (परधर्म के कार्यों में) में लिप्त रहता है वो चेतना रहित होता है और नष्ट हो जाता है। भगवान ऐसे ‘परधर्म’ अनुसरण करने के परिणाम को भयावह कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सांसारिक कर्मों अर्थात परधर्म में संलग्न पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है और वो बार- बार जन्म लेकर संसार चक्र में फंसा रह जाता है । संसार चक्र में फंसा रहना सच में एक भयावह स्थिति है।